सभ्यता का संकट और भारतीय बुद्धिजीवी/ किशन पटनायक
देश की समस्याएं जैसे – जैसे गहरा रही हैं और समाधान समझ के बाहर हो रहा
है , वैसे – वैसे कुछ सोचनेवालों की नजर राजनीति और प्रशासन के परे जाकर
समस्याओं की जड़ ढ़ूंढ़ने की कोशिश कर रही है । वैसे तो औसत राजनेता , औसत
पत्रकार , औसत पढ़ा – लिखा आदमी अब भी बातचीत और वाद – विवाद में सारा दोष
राजनैतिक नेताओं , चुनाव – प्रणाली या प्रशासन के भ्रष्ताचार में ही देखता
है । लेकिन , क्या वही आदमी कभी आत्मविश्लेषण के क्षणों में यह सोच पाता है
कि वह भी उस भ्रष्टाचार में किस तरह जकड़ा हुआ है । वह यह सोच नहीं पाता
है कि वह भी उस भ्रष्टाचार में किस तरह जकड़ा हुआ है । वह यह सोच नहीं पाता
कि किस तरह वह खुद के भ्रष्टाचार को रोक सकता है ।
कुछ लोग अपने को प्रगतिशील मानते हैं । वे कहीं-न-कहीं समाजवादी या साम्यवादी राजनीति से जुड़े हुए हैं । कुछ साल पहले तक ऐसे लोग जोश और जोर के साथ बता सकते थे कि आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा । पिछले वर्षों में उनका यह आत्मविश्वास क्षीण हुआ है । साम्यवादी और समाजवादी कई गुटों में विभक्त हो चुके हैं । उनकी राजनीति के जरिए तीसरी दुनिया का आम आदमी एक नए भविष्य की कल्पना नहीं कर पा रहा है । बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा , सर्वव्यापी भ्रष्टाचार , आदमी की अनास्था जैसी समस्याओं को समझने – समझाने में समाजवादी या साम्यवादियों के पुराने सूत्र और मन्त्र विश्वसनीय नहीं रह गये हैं ।
ऐसी स्थिति में कुछ संवेदनशील दिमागों को यह लगने लगा है कि समस्याओं की जड़ में राजनैतिक अनैतिकता नहीं , अथवा नैतिक गलतियां नहीं , बल्कि सभ्यता का संकट है । चर्चाओं में यह बात बार – बार आने लगी है । प्रसिद्ध विचारक डॉ. जयदेव सेठी ने भी ऐसी ही बात कही है । देश के अंग्रेजी में लिखनेवाले विचारकों में उनका प्रमुख स्थान है । पिछले दिनों उन्होंने गांधी का अध्ययन किया है और वर्तमान के लिए गांधी की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है । कारण , गांधी ने समस्याओं की चुनौती को सभ्यता के स्तर पर लिया । गांधी ने सभ्यता के स्तर पर एक टकराव की रणनीति भी बनाई थी ।
प्रशासन और सत्ता-राजनीति से परे , अर्थव्यवस्था और उत्पादन-व्यवस्था के परे जा कर सभ्यता के परिवर्तन द्वारा समस्याओं का समाधान ढ़ूंढ़ना ही गहराई में जाना और दीर्घकालिक सोच और रणनीति बनाना है । सोचने के इस ढंग को गम्भीरता से लेने के पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी , क्योंकि भारतीय संस्कृति और समाज में रहनेवाला जब गहराई में जाता है , तब वह इतना डूब जाता है कि उसको ऊपर की दुनिया नहीं दिखाई देती । उसके लिए राजनीति , व्यवस्था , संघर्ष , आन्दोलन सब कुछ अप्रासंगिक हो जाते हैं । वह खुद इस सभ्यता के जंजाल से हट जाता है । महर्षि अरविन्द , सन्त विनोबा , अच्युत पटवर्धन , पंडित रामनन्दन मिश्र जैसे लोग संघर्ष की राजनीति से , समस्याओं से दूर चले गए क्योंकि समस्याओं की जड़ बहुत गहराई में जाकर दीखने लगी । भारतीय संस्कृति में यह एक जबरदस्त अवगुण है कि आदमी को गहराई में ले जाने की प्रक्रिया में वह उसे समाज से ही अलग कर देती है । गांधीजी के साथ ऐसा नहीं हुआ । सभ्यता से टकराने के लिए गांधीजी को सारी तात्कालिक समस्याओं से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लड़ना पड़ा । लेकिन , गांधीजी की पचास फीसदी बातें ऐसी हैं , जो एक भारतीय को जड़ और उदासीन बना सकती हैं । खुद गांधीजी व्यवहार में आधुनिक और भारतीय दोनों सभ्यताओं से लड़ रहे थे । लेकिन प्रतिपादन में , लेखन तथा प्रचार में , उनका एक ही निशाना रहा – आधुनिक पश्चिमी सभ्यता । भारतीय सभ्यता और हिन्दू व्यवस्था से उनको हर कदम टकराना पड़ा । मृत्यु भी उसी टकराहट से हुई । लेकिन , हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ बताना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । यह या तो एक प्रकार का छद्म था , या फिर सन्तुलित विचार की कमी थी । इसी कारण अभी तक एक सन्तुलित गांधी-विचार नहीं बन सका है ।
गांधी का व्यवहार सन्तुलित था , किन्तु उनमें वैचारिक सन्तुलन नहीं था । दूसरे लोग जब आधुनिक सभ्यता से टकराते हैं , अक्सर दोनों स्तर पर सन्तुलन खोते हैं । प्राचीन सभ्यता के कुछ प्रतीकों को ढ़ूंढ़ कर वे एक गुफा बना लेते हैं और उसमें समाहित हो जाते हैं । उनके लिए समस्या नहीं रह जाती है , संघर्ष की जरूरत नहीं रह जाती है । अधिकांश भारतीय बुद्धिजीवी यह नहीं जानते कि हमारी ‘सभ्यता का संकट’ क्या है ? उनका एक वर्ग आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को नकार कर या उससे घबराकर प्राचीन सभ्यता के गर्भ में चला जाता है । योग , गो-सेवा या कुटीर उद्योग उनके लिए कोई नवनिर्माण की दिशा नहीं है बल्कि एक सुरंग है , जिससे वे प्राचीन सभ्यता की गोदमें पहुंचकर शान्ति की नींद लेने लगते हैं । बुद्धिजीवियों का दूसरा वर्ग पश्चिमी सभ्यता से आक्रांत रहता है , या घोषित तौर पर उसे अपनाता है । उसको अपनाने के क्रम में पश्चिमी सभ्यता का उपनिवेश बनने के लिए वह अपनी स्वीकृति दे देता है । लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है । हम सब कमोबेश आधुनिक सभ्यता से आक्रांत हैं । उसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकारने की कोशिश करते हैं । लेकिन हमारी रगों में प्राचीन भारतीय सभ्यता का भूत भी बैठा हुआ है । उसके सामने हम बच्चे जैसे भीत या शिथिल हो जाते हैं । वह हमें व्यक्ति या समूह के तौर पर निष्क्रिय , तटस्थ और अप्रयत्नशील बना देता है । जो लोग पश्चिमी सभ्यता को बेहिचक ढ़ंग से अपनाते हैं, वे भी साईं बाबा के चरण-स्पर्श से ही अपनी सार्थकता महसूस करते हैं । सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर मार्क्सवादी रहे हैं और महेश योगी के भक्त भी हैं । नाम लेना अपवाद का उल्लेख करना नहीं है । यह अपवाद नहीं , नियम है । यह विविधता का समन्वय नहीं है , यह केवल वैचारिक दोगलापन है । दोगली मानसिकता की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी पद्धति की होती नहीं और खुद भी कोई पद्धति नहीं बना सकती । दूसरी विशेषता यह होती है कि वह केवल बने बनाये पिंडों को जोड़ सकती है , उनमें से किसी को बदल नहीं सकती , उनमें से किसी को बदल नहीं सकती । तीसरी विशेषता यह है कि वह आत्मसमीक्षा नहीं कर सकती । आत्मसमीक्षा करेगी , तो बने-बनाए पिंडों से संघर्ष करना पड़ेगा । इसलिए बाहर की तारीफ से गदगद हो जाती है और आलोचना को अनसुना कर देती है । इसकी चौथी विशेषता यह है कि वह मौलिकता से डरती है । एक दोगले व्यक्तित्व का उदाहरण होगा ,’श्री आरक्षण-विरोधी जनेऊधारी कम्प्यूटर विशेषज्ञ’ ! इस तरह के व्यक्तित्व को हम क्या कहेंगे – ‘विविधता का समन्वय?’ तो भारतीय बुद्धिजीवी को जब पश्चिमी सभ्यता अधूरी लगती है , तब वह प्राचीनता की किसी गुफा में घुस जाता है और जब वह अपनी सभ्यता के बारे में शर्मिन्दा होता है तब पश्चिम का उपनिवेश बन कर रहना स्वीकार कर लेता है । दोनों सभ्यताओं से संघर्ष करने की प्रव्रुत्ति भारतीय बुद्धिजीवी जगत में अभी तक नहीं विकसित हुई है या जो हुई थी , वह खत्म हो गई है । गांधी के अनुयाई गुफाओं में चले गये। रवि ठाकुर के लोग अंग्रेजी और अंग्रेजियत के भक्त हो गये । गांधी के एक शिष्य राममनोहर लोहिया ने ‘इतिहास चक्र’ नामक एक किताब लिखी । एक नई सभ्यता की धारा चलाने के लिए आवश्यक अवधारणाएं प्रस्तुत करना इस किताब का लक्ष्य था । अंग्रेजी में लिखित होने के बावजूद बुद्धिजीवियों ने उसे नहीं पढ़ा । औपनिवेशिक दिमाग नवनिर्माण की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता । ज्यादा-से-ज्यादा वह प्रचलित और पुरानी धाराओं को साथ-साथ चलाने की कोशिश करता है और दोनों के लिए कम-से-कम प्रतिरोध की रणनीति अपनाता है । आम जनता पर दोनों प्रतिकूल सभ्यताओं का बोझ पड़ता है और वह अपनी तकलीफ के अहसास से आन्दोलित होती है । सभ्यताओं से संघर्ष की इच्छा शक्ति के अभाव में देश के सारे राजनैतिक दल अप्रासंगिक और गतिहीन हो गए हैं । जनता के आन्दोलन को दिशा देने की क्षमता उनमें नहीं रह गई है । जन-आन्दोलनों का केवल हुंकार होता है, आन्दोलन का मार्ग बन नहीं पाता । जहां क्षितिज की कल्पना नहीं है, वहां मार्ग कैसे बने ? इस कल्पना के अभाव में क्रान्ति अवरुद्ध हो जाती है ।
ऐसी स्थिति में यही कहना काफी नहीं होगा कि सभ्यता के स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । मुकाबले की रणनीति भी बनानी पड़ेगी । किन बिन्दुओं पर हम सभ्यता या सभ्यताओं से टकराएंगे ? आधुनिक सभ्यता ने हमें कहां गुलाम बनाया है ? प्राचीन सभ्यता ने हमें कहां दबोच रखा है और पंगु बनाया है ? आज हम किन बिन्दुओं पर किस प्रकार का विद्रोह कर सकते हैं ? इन ठोस सवालों से जो नहीं जूझेगा , वह गांधी की प्रशंसा करेगा तो तो नेहरू का भी समर्थन करेगा । यह एक बौद्धिक बाजीगरी होगी, संघर्ष नहीं होगा,सृजन नहीं होगा । सभ्यताओं से जो तकरायेगा , उसे कुछ झेलना पड़ेगा। अपने वर्ग और तबके में उसे अप्रिय और कटु होना पड़ेगा ।
आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह दुनिया को अपने मानदंडों के अनुसार आधुनिक नहीं बना नहीं सकती । बारी – बारी से वह कुछ इलाकों को प्रलोभित करती है कि ‘ तुमको आधुनिक बना सकती हूं अमरीकी ढंग से नहीं , तो रूसी ढंग से ।’ पूरी दुनिया को एक समय के अन्दर आधुनिक बना सकने का दावा अभी तक वह कर नहीं सकी है। अतः यह सभ्यता दुनिया के बड़े हिस्से को उपनिवेश बना कर ही रख सकती है , जिसके लिए आधुनिक सभ्यता का अर्थ उपभोग का कुछ सामान मात्र है ।
प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ा अपराध यह है कि राष्ट्रीयता और सामाजिक समता के मूल्य उसमें नहीं हैं । जो भारतीय सभ्यता अब बची हुई है , उसकी सारी प्रवृत्ति इन मूल्यों के विरुद्ध है । मनुष्य , मनुष्य की बराबरी या आपसी प्रेम पारम्परिक भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है । ऐसे मनुष्य की संवेदनहीनता , यन्त्र की संवेदनाहीनता से कम खतरनाक नहीं है । मानव के प्रति उदासीनता प्राचीन हिन्दू संस्कृति का गुण था या नहीं , या यह वर्तमान की एक विकृति है , यह स्पष्ट नहीं है । प्राचीन भारतीय मान्यता न सिर्फ सामाजिक समता के विरुद्ध है, बल्कि वह आध्यात्मिक समता की अवधारणा को भी नकारती है । उसके अनुसार कुछ लोगों की आत्मा ही घटिया दरजे की होती है । बुद्ध ने इस मानवविरोधी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश की थी । लेकिन आधुनिक हिन्दू मनुष्य की विरासत में बुद्ध की धारा नहीं है । पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसने मानव की गरिमा और सामाजिक समानता को मूल्यों के तौर पर विकसित किया है । राष्ट्रीयता और अन्तरराष्ट्रीयता की भावना भी इन मूल्यों पर आधारित है । हिन्दू मनुष्य जब तक इन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर लेता है , तब तक वह पश्चिम से बेहतर एक नई सभ्यता बनाने का दावा नहीं कर सकता ।
आधुनिक सभ्यता ने हमें उपनिवेश बनाया है । प्राचीन सभ्यता ने हमें समता विरोधी और मानव विरोधी बनाया है । इन बिन्दुओं पर अगर हम सभ्यता का संघर्ष नहीं चलाते हैं तो हमारी राजनीति , प्रशासन , अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं बदलनेवाली है । इसके बिना हमारे साहित्य , कला , विज्ञान के क्षेत्र में भी कोई उड़ान नहीं हो सकेगी । आधुनिक सभ्यता से संघर्ष की शुरुआत औपनिवेशिक मानस को झकझोरने से होगी । उपभोगवाद , बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और सांस्कृतिक परनिर्भरता को निशाना बनाकर ही यह कार्यक्रम हो सकेगा । दूसरी ओर, हिन्दू मानसिकता और हिन्दू समाज को सुधारने के लिए उग्र कार्यक्रम की जरूरत है ।
मानसिकता कितनी अपरिवर्तित है ही , इसका प्रमाण हरिजनों की प्रतिक्रिया से मिलता है । हाल की घटनाएं बतलाती हैं कि हरिजनों को धर्म-परिवर्तन के लिए बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता है । हरिजनों के लिए मानव का दरजा प्राप्त करने के दो ही रास्ते दीखते हैं – धर्म-परिवर्तन और आरक्षण । आरक्षण का मतलब है हिन्दू मन की उदारता । क्या इस वक्त हिन्दू मन उतनी उदारता के लिए पूरी तरह तैयार है ? जिन दिनों दयानन्द , विवेकानन्द या गांधी हिन्दू समाज के नेता थे , उनका प्रयास और प्रभाव हिन्दू मन को मानवीय बनाने का था । हिन्दू समाज को पिघलाना उनका काम था । जब हिन्दू समाज पिघलता है तब भारतीय राष्ट्र बनता है , हिन्दू समाज जहां जड़ होता है , वहां भारतीय राष्ट्र के सिकुड़ने का डर रहता है ।
दो सभ्यताओं से एक साथ टकराना सत्ता की अल्पकालीन राजनीति में संभव नहीं है । मौजूदा राजनीतिक दलों की क्षमता के अनुसार उनका एकमात्र जायज लक्ष्य हो सकता है – लोकतंत्र के ढांचे की रक्षा करना । अगर ये दल इतना भी नहीं कर सकते तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि सभ्यताओं से लड़े बिना लोकतंत्र की रक्षा सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में आम जनता के विद्रोहों का राजनीतिकरण नहीं होगा । कभी – कभी विद्यार्थियों में , कभी किसानों में , कभी दलितों में , कभी उपेक्षित इलाकों में खंड-विद्रोह होते हैं । इन तबकों और इलाकों पर दोनों सभ्यताओं का बोझ पड़ता है । मौजूदा राजनैतिक दलों का जो वैचारिक ढांचा है , उसमें इन समूहों की मुक्ति हो नहीं सकती । उनकी मुक्ति के लिए एक नया वैचारिक ढांचा चाहिए । जनता के खंड – विद्रोहों और नए वैचारिक ढांचे के सम्मिश्रण से एक नई राजनीति पैदा हो सकती है ।
वैचारिक संघर्ष बुद्धिजीवी ही करेगा । बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है । भारत का बुद्धिजीवी वर्ग अभी मानसिक स्तर पर दोगला ही रहेगा । लेकिन टोलियों में या व्यक्ति के तौर पर बुद्धिजीवी एक नई सभ्यता-निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है । सारे बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे संगठन या हड़ताल चलायें । लेकिन यह अपेक्षा जरूर रहेगी कि आचरण के स्तर पर वे अपने विचार-संघर्ष को झेलें , ताकि विचारों का सामाजिक प्रभाव बने ।
(सामयिक वार्ता , जनवरी ,१९८२ में प्रकाशित)
कुछ लोग अपने को प्रगतिशील मानते हैं । वे कहीं-न-कहीं समाजवादी या साम्यवादी राजनीति से जुड़े हुए हैं । कुछ साल पहले तक ऐसे लोग जोश और जोर के साथ बता सकते थे कि आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा । पिछले वर्षों में उनका यह आत्मविश्वास क्षीण हुआ है । साम्यवादी और समाजवादी कई गुटों में विभक्त हो चुके हैं । उनकी राजनीति के जरिए तीसरी दुनिया का आम आदमी एक नए भविष्य की कल्पना नहीं कर पा रहा है । बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा , सर्वव्यापी भ्रष्टाचार , आदमी की अनास्था जैसी समस्याओं को समझने – समझाने में समाजवादी या साम्यवादियों के पुराने सूत्र और मन्त्र विश्वसनीय नहीं रह गये हैं ।
ऐसी स्थिति में कुछ संवेदनशील दिमागों को यह लगने लगा है कि समस्याओं की जड़ में राजनैतिक अनैतिकता नहीं , अथवा नैतिक गलतियां नहीं , बल्कि सभ्यता का संकट है । चर्चाओं में यह बात बार – बार आने लगी है । प्रसिद्ध विचारक डॉ. जयदेव सेठी ने भी ऐसी ही बात कही है । देश के अंग्रेजी में लिखनेवाले विचारकों में उनका प्रमुख स्थान है । पिछले दिनों उन्होंने गांधी का अध्ययन किया है और वर्तमान के लिए गांधी की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है । कारण , गांधी ने समस्याओं की चुनौती को सभ्यता के स्तर पर लिया । गांधी ने सभ्यता के स्तर पर एक टकराव की रणनीति भी बनाई थी ।
प्रशासन और सत्ता-राजनीति से परे , अर्थव्यवस्था और उत्पादन-व्यवस्था के परे जा कर सभ्यता के परिवर्तन द्वारा समस्याओं का समाधान ढ़ूंढ़ना ही गहराई में जाना और दीर्घकालिक सोच और रणनीति बनाना है । सोचने के इस ढंग को गम्भीरता से लेने के पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी , क्योंकि भारतीय संस्कृति और समाज में रहनेवाला जब गहराई में जाता है , तब वह इतना डूब जाता है कि उसको ऊपर की दुनिया नहीं दिखाई देती । उसके लिए राजनीति , व्यवस्था , संघर्ष , आन्दोलन सब कुछ अप्रासंगिक हो जाते हैं । वह खुद इस सभ्यता के जंजाल से हट जाता है । महर्षि अरविन्द , सन्त विनोबा , अच्युत पटवर्धन , पंडित रामनन्दन मिश्र जैसे लोग संघर्ष की राजनीति से , समस्याओं से दूर चले गए क्योंकि समस्याओं की जड़ बहुत गहराई में जाकर दीखने लगी । भारतीय संस्कृति में यह एक जबरदस्त अवगुण है कि आदमी को गहराई में ले जाने की प्रक्रिया में वह उसे समाज से ही अलग कर देती है । गांधीजी के साथ ऐसा नहीं हुआ । सभ्यता से टकराने के लिए गांधीजी को सारी तात्कालिक समस्याओं से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लड़ना पड़ा । लेकिन , गांधीजी की पचास फीसदी बातें ऐसी हैं , जो एक भारतीय को जड़ और उदासीन बना सकती हैं । खुद गांधीजी व्यवहार में आधुनिक और भारतीय दोनों सभ्यताओं से लड़ रहे थे । लेकिन प्रतिपादन में , लेखन तथा प्रचार में , उनका एक ही निशाना रहा – आधुनिक पश्चिमी सभ्यता । भारतीय सभ्यता और हिन्दू व्यवस्था से उनको हर कदम टकराना पड़ा । मृत्यु भी उसी टकराहट से हुई । लेकिन , हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ बताना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । यह या तो एक प्रकार का छद्म था , या फिर सन्तुलित विचार की कमी थी । इसी कारण अभी तक एक सन्तुलित गांधी-विचार नहीं बन सका है ।
गांधी का व्यवहार सन्तुलित था , किन्तु उनमें वैचारिक सन्तुलन नहीं था । दूसरे लोग जब आधुनिक सभ्यता से टकराते हैं , अक्सर दोनों स्तर पर सन्तुलन खोते हैं । प्राचीन सभ्यता के कुछ प्रतीकों को ढ़ूंढ़ कर वे एक गुफा बना लेते हैं और उसमें समाहित हो जाते हैं । उनके लिए समस्या नहीं रह जाती है , संघर्ष की जरूरत नहीं रह जाती है । अधिकांश भारतीय बुद्धिजीवी यह नहीं जानते कि हमारी ‘सभ्यता का संकट’ क्या है ? उनका एक वर्ग आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को नकार कर या उससे घबराकर प्राचीन सभ्यता के गर्भ में चला जाता है । योग , गो-सेवा या कुटीर उद्योग उनके लिए कोई नवनिर्माण की दिशा नहीं है बल्कि एक सुरंग है , जिससे वे प्राचीन सभ्यता की गोदमें पहुंचकर शान्ति की नींद लेने लगते हैं । बुद्धिजीवियों का दूसरा वर्ग पश्चिमी सभ्यता से आक्रांत रहता है , या घोषित तौर पर उसे अपनाता है । उसको अपनाने के क्रम में पश्चिमी सभ्यता का उपनिवेश बनने के लिए वह अपनी स्वीकृति दे देता है । लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है । हम सब कमोबेश आधुनिक सभ्यता से आक्रांत हैं । उसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकारने की कोशिश करते हैं । लेकिन हमारी रगों में प्राचीन भारतीय सभ्यता का भूत भी बैठा हुआ है । उसके सामने हम बच्चे जैसे भीत या शिथिल हो जाते हैं । वह हमें व्यक्ति या समूह के तौर पर निष्क्रिय , तटस्थ और अप्रयत्नशील बना देता है । जो लोग पश्चिमी सभ्यता को बेहिचक ढ़ंग से अपनाते हैं, वे भी साईं बाबा के चरण-स्पर्श से ही अपनी सार्थकता महसूस करते हैं । सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर मार्क्सवादी रहे हैं और महेश योगी के भक्त भी हैं । नाम लेना अपवाद का उल्लेख करना नहीं है । यह अपवाद नहीं , नियम है । यह विविधता का समन्वय नहीं है , यह केवल वैचारिक दोगलापन है । दोगली मानसिकता की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी पद्धति की होती नहीं और खुद भी कोई पद्धति नहीं बना सकती । दूसरी विशेषता यह होती है कि वह केवल बने बनाये पिंडों को जोड़ सकती है , उनमें से किसी को बदल नहीं सकती , उनमें से किसी को बदल नहीं सकती । तीसरी विशेषता यह है कि वह आत्मसमीक्षा नहीं कर सकती । आत्मसमीक्षा करेगी , तो बने-बनाए पिंडों से संघर्ष करना पड़ेगा । इसलिए बाहर की तारीफ से गदगद हो जाती है और आलोचना को अनसुना कर देती है । इसकी चौथी विशेषता यह है कि वह मौलिकता से डरती है । एक दोगले व्यक्तित्व का उदाहरण होगा ,’श्री आरक्षण-विरोधी जनेऊधारी कम्प्यूटर विशेषज्ञ’ ! इस तरह के व्यक्तित्व को हम क्या कहेंगे – ‘विविधता का समन्वय?’ तो भारतीय बुद्धिजीवी को जब पश्चिमी सभ्यता अधूरी लगती है , तब वह प्राचीनता की किसी गुफा में घुस जाता है और जब वह अपनी सभ्यता के बारे में शर्मिन्दा होता है तब पश्चिम का उपनिवेश बन कर रहना स्वीकार कर लेता है । दोनों सभ्यताओं से संघर्ष करने की प्रव्रुत्ति भारतीय बुद्धिजीवी जगत में अभी तक नहीं विकसित हुई है या जो हुई थी , वह खत्म हो गई है । गांधी के अनुयाई गुफाओं में चले गये। रवि ठाकुर के लोग अंग्रेजी और अंग्रेजियत के भक्त हो गये । गांधी के एक शिष्य राममनोहर लोहिया ने ‘इतिहास चक्र’ नामक एक किताब लिखी । एक नई सभ्यता की धारा चलाने के लिए आवश्यक अवधारणाएं प्रस्तुत करना इस किताब का लक्ष्य था । अंग्रेजी में लिखित होने के बावजूद बुद्धिजीवियों ने उसे नहीं पढ़ा । औपनिवेशिक दिमाग नवनिर्माण की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता । ज्यादा-से-ज्यादा वह प्रचलित और पुरानी धाराओं को साथ-साथ चलाने की कोशिश करता है और दोनों के लिए कम-से-कम प्रतिरोध की रणनीति अपनाता है । आम जनता पर दोनों प्रतिकूल सभ्यताओं का बोझ पड़ता है और वह अपनी तकलीफ के अहसास से आन्दोलित होती है । सभ्यताओं से संघर्ष की इच्छा शक्ति के अभाव में देश के सारे राजनैतिक दल अप्रासंगिक और गतिहीन हो गए हैं । जनता के आन्दोलन को दिशा देने की क्षमता उनमें नहीं रह गई है । जन-आन्दोलनों का केवल हुंकार होता है, आन्दोलन का मार्ग बन नहीं पाता । जहां क्षितिज की कल्पना नहीं है, वहां मार्ग कैसे बने ? इस कल्पना के अभाव में क्रान्ति अवरुद्ध हो जाती है ।
ऐसी स्थिति में यही कहना काफी नहीं होगा कि सभ्यता के स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । मुकाबले की रणनीति भी बनानी पड़ेगी । किन बिन्दुओं पर हम सभ्यता या सभ्यताओं से टकराएंगे ? आधुनिक सभ्यता ने हमें कहां गुलाम बनाया है ? प्राचीन सभ्यता ने हमें कहां दबोच रखा है और पंगु बनाया है ? आज हम किन बिन्दुओं पर किस प्रकार का विद्रोह कर सकते हैं ? इन ठोस सवालों से जो नहीं जूझेगा , वह गांधी की प्रशंसा करेगा तो तो नेहरू का भी समर्थन करेगा । यह एक बौद्धिक बाजीगरी होगी, संघर्ष नहीं होगा,सृजन नहीं होगा । सभ्यताओं से जो तकरायेगा , उसे कुछ झेलना पड़ेगा। अपने वर्ग और तबके में उसे अप्रिय और कटु होना पड़ेगा ।
आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह दुनिया को अपने मानदंडों के अनुसार आधुनिक नहीं बना नहीं सकती । बारी – बारी से वह कुछ इलाकों को प्रलोभित करती है कि ‘ तुमको आधुनिक बना सकती हूं अमरीकी ढंग से नहीं , तो रूसी ढंग से ।’ पूरी दुनिया को एक समय के अन्दर आधुनिक बना सकने का दावा अभी तक वह कर नहीं सकी है। अतः यह सभ्यता दुनिया के बड़े हिस्से को उपनिवेश बना कर ही रख सकती है , जिसके लिए आधुनिक सभ्यता का अर्थ उपभोग का कुछ सामान मात्र है ।
प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ा अपराध यह है कि राष्ट्रीयता और सामाजिक समता के मूल्य उसमें नहीं हैं । जो भारतीय सभ्यता अब बची हुई है , उसकी सारी प्रवृत्ति इन मूल्यों के विरुद्ध है । मनुष्य , मनुष्य की बराबरी या आपसी प्रेम पारम्परिक भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है । ऐसे मनुष्य की संवेदनहीनता , यन्त्र की संवेदनाहीनता से कम खतरनाक नहीं है । मानव के प्रति उदासीनता प्राचीन हिन्दू संस्कृति का गुण था या नहीं , या यह वर्तमान की एक विकृति है , यह स्पष्ट नहीं है । प्राचीन भारतीय मान्यता न सिर्फ सामाजिक समता के विरुद्ध है, बल्कि वह आध्यात्मिक समता की अवधारणा को भी नकारती है । उसके अनुसार कुछ लोगों की आत्मा ही घटिया दरजे की होती है । बुद्ध ने इस मानवविरोधी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश की थी । लेकिन आधुनिक हिन्दू मनुष्य की विरासत में बुद्ध की धारा नहीं है । पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसने मानव की गरिमा और सामाजिक समानता को मूल्यों के तौर पर विकसित किया है । राष्ट्रीयता और अन्तरराष्ट्रीयता की भावना भी इन मूल्यों पर आधारित है । हिन्दू मनुष्य जब तक इन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर लेता है , तब तक वह पश्चिम से बेहतर एक नई सभ्यता बनाने का दावा नहीं कर सकता ।
आधुनिक सभ्यता ने हमें उपनिवेश बनाया है । प्राचीन सभ्यता ने हमें समता विरोधी और मानव विरोधी बनाया है । इन बिन्दुओं पर अगर हम सभ्यता का संघर्ष नहीं चलाते हैं तो हमारी राजनीति , प्रशासन , अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं बदलनेवाली है । इसके बिना हमारे साहित्य , कला , विज्ञान के क्षेत्र में भी कोई उड़ान नहीं हो सकेगी । आधुनिक सभ्यता से संघर्ष की शुरुआत औपनिवेशिक मानस को झकझोरने से होगी । उपभोगवाद , बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और सांस्कृतिक परनिर्भरता को निशाना बनाकर ही यह कार्यक्रम हो सकेगा । दूसरी ओर, हिन्दू मानसिकता और हिन्दू समाज को सुधारने के लिए उग्र कार्यक्रम की जरूरत है ।
मानसिकता कितनी अपरिवर्तित है ही , इसका प्रमाण हरिजनों की प्रतिक्रिया से मिलता है । हाल की घटनाएं बतलाती हैं कि हरिजनों को धर्म-परिवर्तन के लिए बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता है । हरिजनों के लिए मानव का दरजा प्राप्त करने के दो ही रास्ते दीखते हैं – धर्म-परिवर्तन और आरक्षण । आरक्षण का मतलब है हिन्दू मन की उदारता । क्या इस वक्त हिन्दू मन उतनी उदारता के लिए पूरी तरह तैयार है ? जिन दिनों दयानन्द , विवेकानन्द या गांधी हिन्दू समाज के नेता थे , उनका प्रयास और प्रभाव हिन्दू मन को मानवीय बनाने का था । हिन्दू समाज को पिघलाना उनका काम था । जब हिन्दू समाज पिघलता है तब भारतीय राष्ट्र बनता है , हिन्दू समाज जहां जड़ होता है , वहां भारतीय राष्ट्र के सिकुड़ने का डर रहता है ।
दो सभ्यताओं से एक साथ टकराना सत्ता की अल्पकालीन राजनीति में संभव नहीं है । मौजूदा राजनीतिक दलों की क्षमता के अनुसार उनका एकमात्र जायज लक्ष्य हो सकता है – लोकतंत्र के ढांचे की रक्षा करना । अगर ये दल इतना भी नहीं कर सकते तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि सभ्यताओं से लड़े बिना लोकतंत्र की रक्षा सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में आम जनता के विद्रोहों का राजनीतिकरण नहीं होगा । कभी – कभी विद्यार्थियों में , कभी किसानों में , कभी दलितों में , कभी उपेक्षित इलाकों में खंड-विद्रोह होते हैं । इन तबकों और इलाकों पर दोनों सभ्यताओं का बोझ पड़ता है । मौजूदा राजनैतिक दलों का जो वैचारिक ढांचा है , उसमें इन समूहों की मुक्ति हो नहीं सकती । उनकी मुक्ति के लिए एक नया वैचारिक ढांचा चाहिए । जनता के खंड – विद्रोहों और नए वैचारिक ढांचे के सम्मिश्रण से एक नई राजनीति पैदा हो सकती है ।
वैचारिक संघर्ष बुद्धिजीवी ही करेगा । बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है । भारत का बुद्धिजीवी वर्ग अभी मानसिक स्तर पर दोगला ही रहेगा । लेकिन टोलियों में या व्यक्ति के तौर पर बुद्धिजीवी एक नई सभ्यता-निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है । सारे बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे संगठन या हड़ताल चलायें । लेकिन यह अपेक्षा जरूर रहेगी कि आचरण के स्तर पर वे अपने विचार-संघर्ष को झेलें , ताकि विचारों का सामाजिक प्रभाव बने ।
(सामयिक वार्ता , जनवरी ,१९८२ में प्रकाशित)

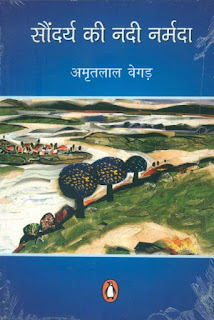








टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें