ईको रूम है सोशल मीडिया, खत्म कर रहा लोकतांत्रिक सोच
 |
| pawel kuczynski |
इसके लोकतांत्रिक होने का पहला मजाक तो डेटा के हेरफेर ने कर दिया। यह बात शत प्रतिशत साबित हो चुकी है। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप से लोगों का विचार बदलना हो या फिर ब्रिटेन में चल रहे ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में । ऐसी घटनाओं ने इस टेक बेस्ड डेमोक्रेसी की सीमाओं का खुलासा कर दिया है। यह साफ साफ बता रहा है कि सोशल मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी की लगाम किसी और के हाथ में है। यह पूरा मॉडल कंप्यूटेशनल प्रपोगंडा का है।
सोशल मीडिया का एल्गोदिरदम कुछ इस तरह का इको सिस्टम बनाता है कि उसमें हमारी सोच से अलग कुछ ऐसा होता ही नहीं, जो हमें चुनौती दे सके। कभी गलती से कोई भूला-भटका आ गया तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे वैकल्पिक आत्मीयता या सेलेक्टिव एक्सपोजर कहते हैं। ऐसी स्थिति तब बनती है जब हमारे सामने यह विकल्प हो कि किस पर भरोसा करें या अपना पक्ष चुन लें। सोशल मीडिया पर जो सूचनाएं सामने आती हैं, वह वही होती हैं जिनको हम पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे अपने चुने हुए पक्ष को मजबूत करती हैं। यह समस्य तो आम है कि हम एक कम्युनिटी साइलो का निर्माण करते हैं। मनुष्य हमेशा से ऐसा ही करना चाहता है। असल चुनौती तो यह है कि सोशल मीडिया नेटवर्क हमें एक बबल बॉय बनाता है। यह हमें उन राजनीतिक या सांस्कृतिक विचारों से पूरी तरह महफूज रखता है जो हमसे भिन्न हैं। यह यूजर को खास तरह का भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सब मिलकर एक ऐसा स्पेस बनाता है कि न तो हमें बाहर की कोई खबर लगती है और न ही हम इससे निकल पाते हैं। बस इसमें तैरते रहते हैं। यह किसी ईको चैंबर की तरह है। हम जो बात लिखते-बोलते हैं वही प्रतिध्वनित होकर हमारे आसपास गूंजती है।
अमेरिका में जब नवंबर 2016 में चुनाव खत्म हुआ उसके तुरंत बाद मुस्तफा अल बरमावे ने एक लेख लिखा था। जिसमें उन्होंने यह बात कही थी कि फेसबुक और गूगल के सोशल बबल्स नई तरह की वास्तविकताएं गढ़ रहे हैं। हम सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो हमें पसंद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आपके भीतर के लोकतांत्रिक ख्याल को नष्ट कर रहा है। वे कहते हैं कि इसने ग्लोबल विलेज कंसेप्ट को रिप्लेस करके डिजिटल आइलैंड को जगह दे दिया है। जो कि एक दूसरे से बिल्कुल संबद्ध नहीं हैं। वे हर दिन अलग-अलग दिशा में बह रहे हैं।
यह सब देखकर स्टीफन किंग के उपन्यास अंडर द डोम की याद दिलाता है। उपन्यास की कहानी एक रहस्यमी संरचना के इर्द गिर्द घूमती है। जो कि अचनाक एक छोटे से शहर को पूरी तरह कवर कर लेता है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। टाउन वाले जल्द ही कई गुटों में बंट जाते हैं। इसमें रहने वाले प्रगतिशील लोग खुद को अमेरिका का प्रथम नागरिक कहे जाने वालों से प्रताड़ित महसूस करते हैं। वे भले ही एक ही गुंबद के नीचे फंसे हैं लेकिन उनमें एक दूसरे से प्रभावी संवाद का कोई तरीका नहीं है। अंत में दोनों पक्ष पागल हो जाते हैं।
हालांकि मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया का बुलबुला या इको चैंबर लोकतांत्रिक विचार को पूरी तरह खत्म कर पाएगा कभी। लेकिन इतना तो तय है कि यह हमारी अंतर को समझने की क्षमता को बहुत सीमित कर देगा। यदि हम जो देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं वही करते हैं तो हम नागरिक और मनुष्य के रूप में बौने जाएंगे।
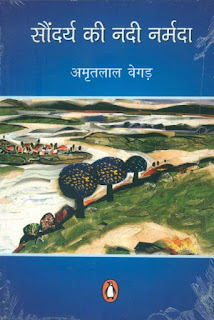







टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें